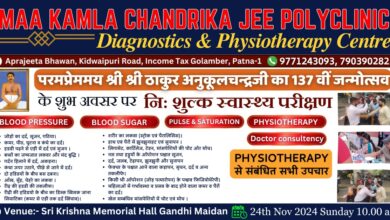जीवन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए श्रेय का मार्ग ही श्रेयस्कर


-मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा में संपन्न हुआ आनन्द मार्ग का तीन दिवसीय
संभागीय सेमिनार
फोटो-
जहानाबाद।
मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा में आनन्दमार्ग प्रचारक संघ द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित तीन दिवसीय आवासीय संभागीय सेमिनार के अवसर पर अंतिम दिन रविवार को अमेरिका समेत कई देशों में आनंद मार्ग के विचारों और सिद्धान्तों का प्रसार करने वाले आनन्दमार्ग के वरिष्ठ आचार्य सिध्द विद्यानंद अवधूत ने “*श्रेय और प्रेय”* विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि “श्रेय और प्रेय, मानव जीवन के दो प्रमुख पहलू हैं जो हमारे विचार, कार्य और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। *श्रेय वह मार्ग है, जो हमें आत्मिक उत्थान और अनन्त सुख की ओर ले जाता है,* जबकि प्रेय वह है जो तात्कालिक सुख और भौतिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे आत्मिक संतोष या स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्रेय का अनुसरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानता है और यात्रा पथ को एक उच्चतर उद्देश्य की दिशा में समर्पित करता है। वह व्यक्ति उन कार्यों और आचरणों में लीन रहता है जो समाज के भले के लिए होते हैं और जो उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समृद्ध करते हैं। इसके विपरीत, प्रेय का मार्ग तात्कालिक भोग-विलास की ओर प्रेरित करता है, जो कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकता और व्यक्ति को केवल अस्थिरता और भौतिकता के जाल में फंसा देता है। आचार्य ने यह भी बताया कि हमारे जीवन में चयन हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर हम श्रेय को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और सम्पूर्ण मानवता के लिए भी एक सशक्त योगदान देते हैं। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। आध्यात्मिक दृष्टि से, श्रेय का मार्ग सहज और स्वाभाविक होता है क्योंकि इसमें आत्म-नियंत्रण, तपस्या और त्याग की आवश्यकता होती है, इसके परिणामस्वरूप शांति, संतोष और अनमोल सुख मिलती है। इसलिए *हमें हमेशा श्रेय के मार्ग को चुनना चाहिए, क्योंकि वही हमारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाता है* और हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति कराता है। आचार्य ने कहा कि नैतिक नियमों (यम- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और नियम- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान) का कठोरता से पालन श्रेय जीवन की आधारशिला है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि साधन है। इस मौके पर आचार्य चिदम्बरानंद अवधूत, यतीन्द्रानंद अवधूत, आचार्य चन्देशानंद अवधूत, अवधूतिका आनंद स्नेहमया आचार्य, सीताराम जी, परमेश्वर जी, चितरंजन जी, नवीन चंद्र प्रसाद भदानी, लक्ष्मीपति नाथ, शैलेंद्र जी, शंभू जी, डॉक्टर संजय जी, गुंजन कुमार, अजय शंकर समेत काफी संख्या में आनंद मार्ग से जुड़े लोग उपस्थित थे।
*दिव्यता की प्राप्ति उपलब्धि है*
आध्यात्मिक यात्रा में, परम सत्ता या परमपुरुष को व्यक्त करने की चुनौती अत्यंत गहरी है। प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान में यह कहा गया है कि जो गुरु परम सत्ता को समझाने का प्रयास करता है, वह इसे सीधे तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द और प्रतीक स्वाभाविक रूप से सापेक्ष होते हैं। इसलिए, इस अंतर को पाटने के लिए, गुरु “मूक” हो जाता है और शिष्य “बहरा”, क्योंकि परम सत्ता भाषा और प्रतीकों से परे है।कृष्णाचार्य के उपदेश एक अनूठा समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे बहरा और मूक व्यक्ति सूक्ष्म संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक साधक अपनी अभिव्यक्ति के लिए अधिक सूक्ष्म प्रतीकात्मक रूपों का उपयोग कर सकते हैं। ये सूक्ष्म प्रतीकात्मकताएँ पारंपरिक संचार विधियों से परे हैं और मन और आत्मा की गहरी अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत करती हैं।
प्रतीकात्मकता की अवधारणा मानव अनुभव को समझने के लिए केंद्रीय है। विचार और भावनाएँ या संस्कार मन में सुप्त प्रतीकों के रूप में विद्यमान रहती हैं जब तक कि वे भौतिक रूप से व्यक्त नहीं होतीं। ये प्रतीक अक्सर पिछले जन्मों से विरासत में आते हैं, जो पुनर्जन्म के चक्र में योगदान करते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके अव्यक्त मानसिक प्रतीक जमा होते रहते हैं, जो भौतिक क्षेत्र में लम्बे समय तक रहने का कारण बनते हैं। हालाँकि, अभिव्यक्ति का ब्रह्मांड विशाल है और मानव चेतना इसे केवल एक छोटे हिस्से को ही समझ पाती है। हमारे अंग और मन ब्रह्मांडीय प्रतीकात्मकता का केवल एक अंश पकड़ पाते हैं, और इसे व्यक्त करने की हमारी क्षमता भी सीमित होती है। फिर भी, कला, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक रूपों के माध्यम से, व्यक्ति अपनी आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अभिव्यक्तियाँ, चाहे वे मानसिक हों या भौतिक, ब्रह्मांडीय मन पर निर्भर होती हैं, जो अप्रकट ब्रह्मांड है और सृजन की पूरी संभावना को अपने भीतर समाहित किए हुए है। मानसिक प्रतीकों की सीमाओं को पार करने के लिए, व्यक्तियों को अपनी मानसिक ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रवाह में संचारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह प्रक्रिया उनके प्रतीकों को मानसिक-आध्यात्मिक तरंगों में रूपांतरित करती है, जो भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता से परे होती है और उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाती है।
इस रूपांतरण का अंतिम उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष है। जब किसी के मानसिक प्रतीकात्मकता को मानसिक-आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता में रूपांतरित किया जाता है, तो उसे भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, और मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। मुक्ति मानव आकांक्षाओं का शिखर है, और यह कोई दूर का भविष्य नहीं है—यह इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है, यदि कोई अपने मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ पुनः संरेखित करता है। जो इस मार्ग को समझ चुके हैं, उनके लिए कार्य स्पष्ट है: मानसिक प्रतीकों को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की ओर निर्देशित करें और इस जीवन में मुक्ति की संभावना को अपनाएं। अनंत प्रतीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है—सच्ची मुक्ति अब हमारे पहुंच में है।
*मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक*
आनन्द मार्ग के आचार्य सिध्द विद्यानंद अवधूत ने पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए बताया कि जल संरक्षण और सतत भूमि प्रबंधन के हमारे दृष्टिकोण को फिर से सोचना और बेहतर बनाना अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए एक संगठित प्रयास जल संकट और पर्यावरणीय गिरावट को प्रभावी रूप से हल कर सकता है।आचार्य ने चार मुख्य बिंदुओं कि चर्चा करते हुए कहा कि पारंपरिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक फसल प्रबंधन का एकीकरण: जैसे बार्ली और सब्जियों जैसी फसलों को एक साथ उगाना जल का प्रभावी उपयोग करने में मदद कर सकता है, जिससे जल अपव्यय को कम किया जा सकता है और जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। बार्ली को सब्जियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, और बहते पानी से फसलों को बिना विशेष बुनियादी ढांचे के सिंचाई की जा सकती है। जल संरक्षण के लिए वृक्षों की रणनीतिक रोपाई: विशेष रूप से फलदार वृक्षों को नदी किनारों और कृषि क्षेत्रों के पास लगाना मिट्टी में पानी बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे नदियाँ और झीलें सूखने से बच सकती हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि पानी वृक्षों की जड़ प्रणालियों में संग्रहित हो और धीरे-धीरे जारी हो, जिससे स्थानीय जल निकायों और आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्रों की सेहत बनी रहती है। वनों और नदी प्रणालियों की पुनर्स्थापना: नदी किनारों पर वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण कई नदियाँ सूख चुकी हैं, जैसे कि बंगाल की मयूराक्षी नदी। पहले इन नदियों के माध्यम से बड़े जहाजों का आवागमन होता था, लेकिन अब जल प्रवाह कम होने के कारण केवल छोटे जहाज ही इन नदियों में चल सकते हैं। वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापना जल चक्रों को स्थिर करने और हमारे जल संसाधनों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन: तालाबों, झीलों और जलाशयों जैसे मौजूदा जल भंडारण प्रणालियों की गहराई और क्षेत्रफल को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधों की संख्या बढ़ाकर और छोटे पैमाने पर जलाशयों का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है। सतही जल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर हम एक अधिक लचीला और सतत जल प्रणाली बना सकते हैं।